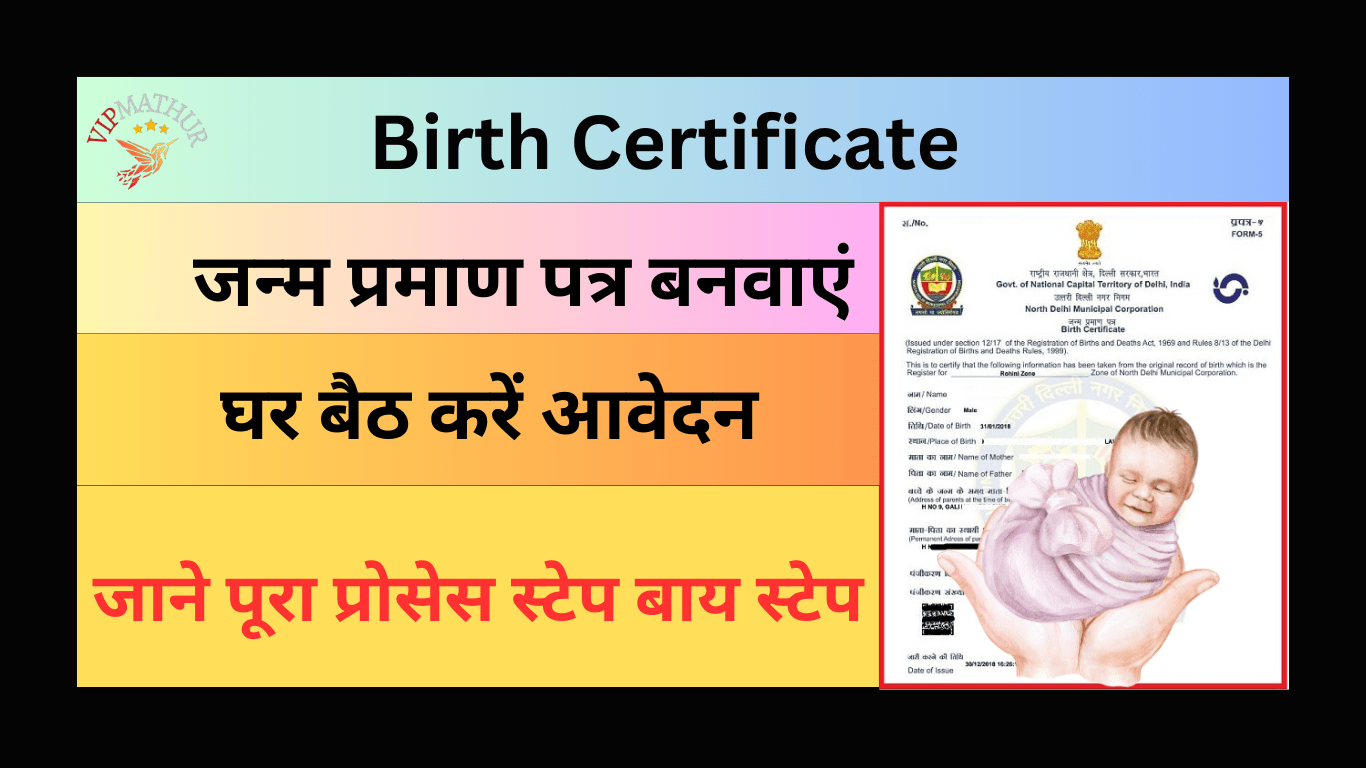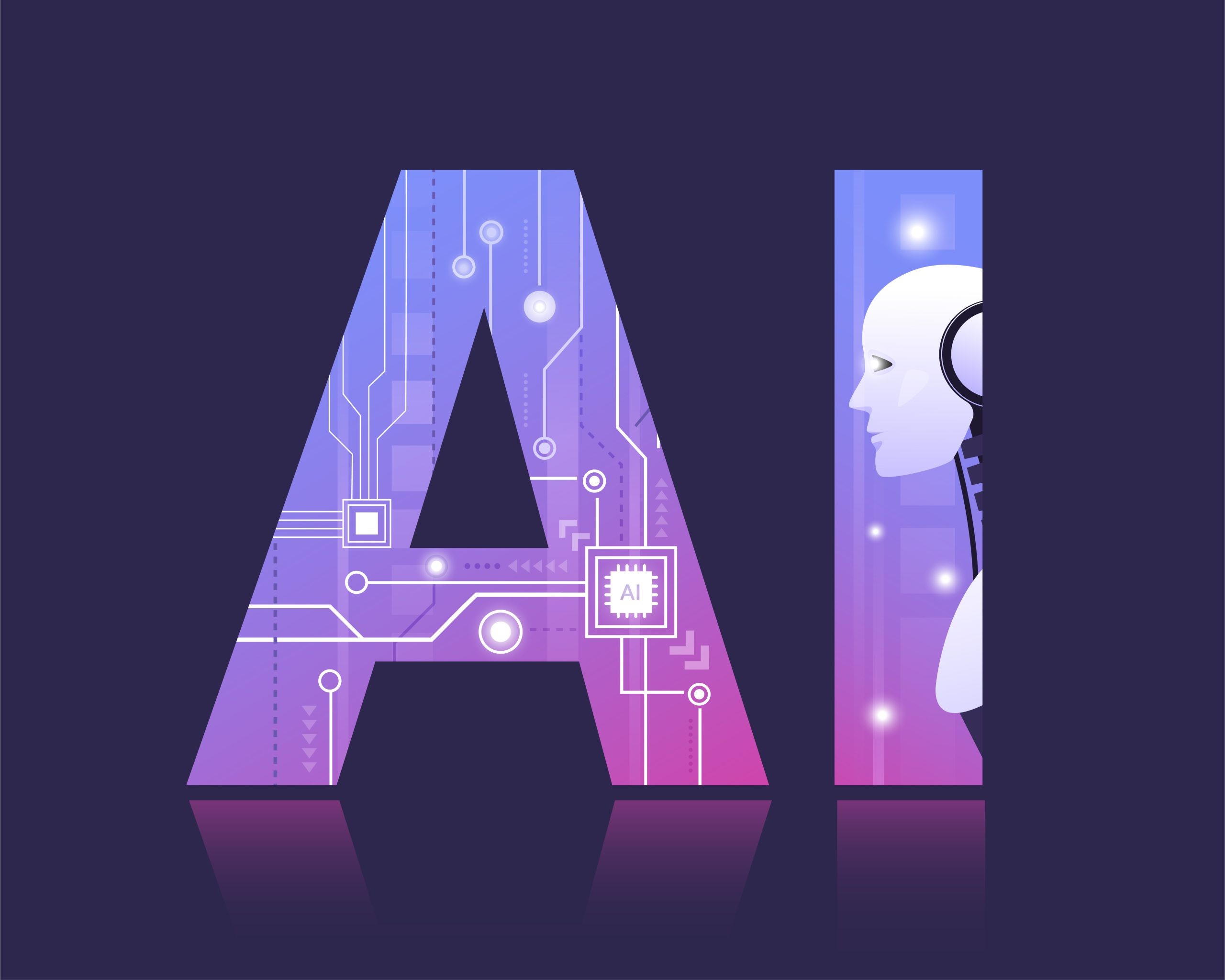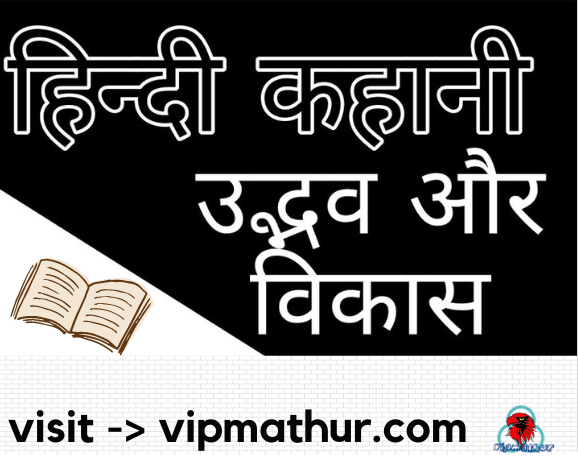निबन्ध के तत्त्वों के आधार पर ‘मेले का ऊँट’ निबन्ध की समीक्षा कीजिए।
मेले का ऊँट निबन्ध की समीक्षा-> मेले का ऊँट’ बालमुकुन्द गुप्त का प्रसिद्ध निबन्ध है। बालमुकुन्द गुप्त के लेख और निबन्ध प्रायः ‘भारतमित्र’ पत्र में प्रकाशित होते थे। इन लेखों और निबन्धों में वे दैनिक जीवन से समस्याएँ और वृत्तों का चयन करके उसकी सामाजिक-राजनीतिक, पर सामायिक व्याख्या करते थे। लॉर्ड कर्जन पर आक्षेप करने का कोई मौका वे नहीं गँवाते थे। आलोच्य -निबन्ध इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। इस निबन्ध में उन्होंने पुराने ज़माने में ऊँट के महत्त्व, वर्तमान में उसकी उपेक्षा, मारवाड़ियों के आधुनिक संस्कृति में डूबने और विश्व की प्रगति तथा लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य को विशेष रूप से ध्यान में रखा है। आलोच्य-निबन्ध की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
1. रोचकता
रोचकता ललित-निबन्ध का प्रधान-तत्त्व है। यदि निबन्ध रोचक नहीं होगा तो पाठक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित ही नहीं कर पाएगा। निबन्ध को रोचक बनाने के लिए कुछ घटनाओं, प्रसंगों आदि का ध्यान कर उ निबन्ध में संजोता है। निबन्ध में शैली की भी प्रस्तुति की दृष्टि से रोचक बनाने का प्रयास करता है। ‘मेले का ऊँट’ पर्याप्त रोचक निबन्ध है। इस निबन्ध का शीर्षक ही पाठक को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। बीच-बीच में लेखक और ऊँट के कथन और कथन-शैली की भंगिमा भी इसे रोचक बनाते चलते हैं। एक उदाहरण देखिए-“बहुत से लोग ऊँट की ओर देखते और हँसते थे। कुछ लोग कहते थे कि कलकत्ते में ऊँट नहीं होते इसी से मोहन मेले वालों ने इस विचित्र जानवर का दर्शन कराया है। बहुत-सी शौकीन बीबियाँ, कितने ही फूल बाबू ऊँट का दर्शन करके झुककर उस काठ के घेरे में बैठे हुए ऊँट की तरफ देखने लगे। एक ने कहा, “ऊँटड़ो है”, दूसरा बोला ‘ऊँटड़ो कठे ते आयो?’ ऊँट ने भी यह देख दोनों होठों को फड़फड़ाते हुए थूथनी फटकारी।”
2. भावात्मकता
भावात्मकता भी निबन्ध का प्रमुख तत्त्व है। वस्तुतः यही वह तत्त्व है। जिसके माध्यम से पाठक लेखक के साथ तादात्म्य स्थापित कर पाता है। यह तत्त्व निबन्ध को रोचक भी बनाता है और सरस भी। प्रस्तुत निबन्ध में भावात्मकता का पूर्ण निर्वाह हुआ है। कुछेक स्थलों कपर लेखक स्वयं भावुक-सा हो जाता है। पाठक भी उसके साथ भाव की तरंग में बह जाता है-“भंग की तरंग में मैंने सोचा कि ऊँट अवश्य ही मारवाड़ी बाबुओं से कुछ कहता है। जो में सोचा कि चलो देखें वह क्या कहता है? क्या उसकी भाषा मेरी समझ में न आवेगी। मारवाड़ियों की भाषा समझ लेता हूँ तो मारवाड़ के ऊँट की बोली साफ-साफ समझ में आने लगी।”
3. सजीवता
सजीवता निबन्ध के प्रमुख तत्त्वों में से एक है। निबंध की सजीवता उसकी सफलता का भी प्रमाण है। निबन्ध में सजीवता रोचक घटनाओं, प्रसंगों से तो आती ही हैं, विषय की सूक्षम और गहन पकड़, भावपूर्णता और कुशल प्रस्तुति भी उसे सजीव बनाती है। ‘मेले का ऊँट’ निश्चय ही एक सजीव निबन्ध बन पड़ा है। पाठक लेखक के साथ-साथ विषय से भी तदातम्य करता है। मेले के ऊँट के साथ उसकी भावनाएँ जुड़ जाती हैं। उसकी उपेक्षा से वह आहत होता है और उसकी सेवाओं के प्रति नत-मस्तक – “तुम्हारी भक्ति घट जाने पर भी मेरा वात्सल्य नहीं घटता है। घटे कैसे, मेरा तुम्हारा जीवन एक ही रस्सी में बँधा हुआ था। मैं ही हल चलाकर तुम्हारे खेतों में अन्न उपजाता था और मैं ही चारा आदि पीठ पर लादकर तुम्हारे घर पहुँचाता था। यहाँ कलकत्ते में जल की कलें हैं, गंगाजी हैं, जल पिलाने को ग्वाले कहार हैं, पर तुम्हारी जन्म-भूमि में मेरी पीठ कर लादकर कोसों से जल आता था और तुम्हारी प्यास बुझाता था।”
4. वैयक्तिकता
वैयक्तिकता निबन्ध, विशेषतः ललित-निबन्ध का प्रमुख तत्त्व माना जाता है। पश्चिम में तो इसे निबन्ध का प्रधान तत्त्व माना ही जाता है, हिन्दी निबन्धों में भी इसके महत्त्व को भली-भाँति समझा और स्वीकारा गया है। वैयक्तिकता के माध्यम से लेखक का पाठक के साथ सहज सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। आलोच्य-निबन्ध में यह बात स्पष्ट रूप से लक्ष्य की जा सकती है। निबन्ध में वैयक्तिकता का समावेश लेखक के भावों-विचारों आदि के माध्यम से तो होता ही है, लेखक की शैली भी इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ‘मेले का ऊँट’ में ऊँट और लेखक की आत्म-कथात्मक शैली इस वैयक्तिकता का मरुदण्ड बनकर आई है। निबन्ध के प्रारम्भ में ही इस वैयक्तिकता को लक्ष्य किया जा सकता है-“भारतमित्र सम्पादक! जीते रहो-दूध-पताशे पीते रहो। भाँग भेजी सो अच्छी थी। फिर वैसी ही भेजना। गत सप्ताह अपना चिट्ठा अपने पत्र में टटोलते हुए ‘मोहन मेले’ के लेख पर निगाह पड़ी। पढ़कर आपकी दृष्टि पर अफसोस हुआ। पहली बार आपकी बुद्धि पर अफसोस हुआ था। भाई……”
5. एकसूत्रता
एकसूत्रता किसी भी निबन्ध का प्राण-तत्त्व होता है। यही वह माध्यम है, जो ललित निबन्धकार को भटकने नहीं देता है। निबन्धकार एक विषय की चर्चा करते समय अन्यत्र भी जा सकता है, ललित निबन्ध में इसका अवकाश भी रहता है। परन्तु वह भी मूल विषय अथवा केन्द्र से संबद्ध होना चाहिए। ‘मेले का ऊँट’ एकसूत्रता का श्रेष्ठ उदाहरण है। संक्षिप्त-सो भूमिका के बाद लेखक मूल विषय पर आ जाता है। मेले के अन्य आकर्षणों के मध्य ऊँट, वर्तमान युग में ऊँट की उपेक्षा, ऊँट द्वारा हर क्षेत्र में मारवाड़ियों की सेवा का वर्णन करने के बाद लेखक बताता है कि वर्तमान में ऊँट का महत्त्व कम होने का कारण भौतिक प्रगति है। विश्व में गति और समृद्धि बढ़ रही है, ऐसे में ऊँट धीरे-धीरे अजायबघर की वस्तु होता जा रहा है। इसी वर्णन के दौरान लेखक लॉर्ड कर्जन की संवेदनशून्यता पर व्यंग्य करता चलता है। इस निबन्ध की विशेषता यह है कि लेखक आदि से अंत तक मूल विषय पर ही ध्यान केन्द्रित रखता है, वह विषयोत्तर होता ही नहीं।
6. हास्य-व्यंग्य
ललित निबन्ध में हास्य-व्यंग्य का भी पर्याप्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। हास्य-व्यंग्य निबन्ध को रोचक बनाता है, उसके कथ्य को प्रभावी बनाता है। हास्य निबन्ध को अधिक सरस एवं पठनीय बनाता है तथा व्यंग्य बुराइयों और विषमताओं के प्रति तीक्ष्ण व कटु भाव पाठक के मन में पैदाकर विषय को प्रभावी बनाता है। ‘मेले का ऊँट’ में लेखक ने इस तत्त्व का भी ध्यान रखा है। कहीं वह ऊँट के प्रति मारवड़ियों की प्रतिक्रिया और कहीं ऊँट की बलबलाहट की तुलना मारवाड़ियों की पत्नी की आवाज़ से करके हल्का हास्य उत्पन्न करता है और कहीं, लॉर्ड कर्जन के प्रति उसका आक्रोश मुखर हो जाता है-“जिस प्रकार लॉर्ड ने किसी जमाने के ‘ब्लैक होल’ को उस पर लाट बनवाकर और उसे संगमरमर से मढ़वाकर शानदार बना दिया है उसी प्रकार मारवाड़ी तुम्हारे लिए मख़मली, ज़री की गद्दियाँ, हीरे-पन्ने की नकेल और सोने की घंटियाँ बनवाकर तुम्हें बड़ा करेंगे और अपने बड़ों की सवारी का सम्मान करेंगे।”
7. काव्यात्मकता
काव्यात्मकता ललित-निबन्ध का मुख्य तत्त्व है। गद्यकार की कसौटी निबन्ध में सर्वत्र काव्यात्म कता न तो अनिवार्य है और न ही अपेक्षित किन्तु यत्र-तत्र इसका समावेश निबन्ध में लालित्य का समावेश करता है। ‘मेले का· ऊँट’ में लेखक का ध्यान भाषा के सह, सरल प्रयोग द्वारा स्वाभाविक हास्य और चुटीले व्यंग्य पर तो गया है किन्तु काव्यात्मकता की प्रवृत्ति उसमें अधिक नहीं आ पाई है। यत्र-तत्र उसकी हल्की-सी झलक भर देखी जा सकती है-“मेरी बलबलाहट उनके कानों को इतनी सुरीली लगती थी कि तुम्हारे बगीचे में तुम्हारें गवैयों तथा तुम्हारी पसन्द की बीबियों के स्वर भी तुम्हें उतने अच्छे न लगते। होंगें। मेरे गले के घण्टों का शब्द उनको सब बाजों में प्यारा लगता था। फोग के जंगल में मुझे चरते देखकर वह उतने प्रसन्न होते थे जितने तुम अपने सजे बगीचों में भंग पीकर, पेट भरकर और ताश खेलकर।”
8. आलंकारिकता
आलंकारिकता भी निबन्ध का प्रमुख तत्त्व है। इसके माध्यम से वर्ण्य-विषय को इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि वह अधिक सहज, ग्राह्य और प्रभावी हो जाता है। उसकी चमत्कारिकता विषय का प्रभाव चित्त पर स्थायी बनाती है। पन्ध फो अधिक ललित और रोचक बनाने का काम भी यह करती है और प्रस्तुति का काव्यात्मक भी बनाती है। आलोच्य-निबंध में काव्यात्मकता की. अल्पता यह संकेत करती है कि आलंकारिकता के व्यर्थ मोह से लेखक बचा है, परन्तु इसकी जानबूझकर उपेक्षा उसने नहीं की है। आलंकारिकता का समावेश यहाँ सहज रूप में ही हो पाया है-“मैंने ऊँट से कहा-बस बलबलाना बंद करो। यह बावला शहर नहीं जो तुम्हें परमेश्वर समझे। तुम पुराने हो तो क्या तुम्हारी कोई कल सीधी नहीं है जिनके पिता स्टेशन से गठरी आप ढोकर लाते थे, उनको सिर पर पगड़ी संभालना भारी है, जिनके पिता का कोई पूरा नाम लेकर नल पुकारता था वही बड़ी-बड़ी उपाधियाँ धारे हुए हैं। संसार का जब यही रंग है तो ऊँट पर चढ़ने वाले सदा ऊँट पर ही चढ़ें यह कुछ बात नहीं।”

9. कलात्मकता
कलात्मकता से तात्पर्य विषय के अभिव्यक्ति-पक्ष से है। ललित-निबंध की भाषा का सरल, एवं विषयानुकूल होना आवश्यक है। आलोच्य निबंध का सशक्त पक्ष इसकी भाषा ही है। आत्म-कथात्मक शैली में लिखे गए इस निबंध की भाषा विषय और पात्रों के अनुकूल ही है। मारवाड़ी यदि ‘ऊँटड़ो’ और ‘ऊँटड़ो कठे ते आयो’ आदि कहते हैं तो ऊँट के संदर्भ में धूंथनी और बलबलाहट जैसे शब्द अभिव्यक्ति को यथार्थ बनाते हैं। भाषा सामान्यतः तद्भव प्रधान, सरल, सरस है किन्तु अंग्रेजी और अरबी-फारसी के शब्दों से लेखक को परहेज नहीं है। ‘पोतड़ो के अमीर’ जैसे मुहावरों का प्रयोग भाषा को अतिरिक्त सक्षमता एवं अर्थवत्ता प्रदान करता है। गुप्त जी की भाषा का एक उदाहरण द्रष्टव्य है -“किसी की पुरानी बातें यों खोलकर कहने से आजकल के कानून से हदतक इज्जत होती है। तुम्हें ख़बर नहीं कि अब मारवाड़ियों ने ‘एसोसिएशन’ बना ली है। अधिक बलवरला वह रिजोल्यूशन पास करके तुम्हें मारवड़ से निकलवा देंगे।”
10. निष्कर्ष
स्पष्ट है कि ‘मेले का ऊँट’ में निबन्ध के सभी तत्त्वों का सम्यक् निर्वाह हुआ है। हिन्दी के प्रारम्भिक दौर के निबन्धकार होते हुए भी गुप्त जी ने हिन्दी की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए सटीक विषय का चयन किया है और उसे युग की आवश्यकताओं के अनुरूप अभिव्यक्ति दी है। भाषा उनके निबन्धों का सशक्त पक्ष है। इनके विषय में रामचन्द्र शुक्ल का कथन है, “उनकी भाषा उर्दू की रवानी है और उनके विचार ‘विनोदपूर्ण वर्णनात्मक विधान’ में लिपटे हैं।” गुप्त जी हिन्दी के निबन्धकारों के लिए श्रेष्ठ आधार सिद्ध हुए हैं, यह बात ‘मेले का अँट’ निबन्ध से पूर्णतया सिद्ध हो जाती है।
मेले का ऊँट निबन्ध की समीक्षा
mele ka oont nibandh kee sameeksha
मेले का ऊँट निबन्ध की समीक्षा
mele ka unt nibandh kee sameeksha
निबन्ध के तत्त्वों के आधार पर ‘मेले का ऊँट’ निबन्ध की समीक्षा कीजिए।
निबन्ध के तत्त्वों के आधार पर ‘मेले का ऊँट’ निबन्ध
मेले का ऊँट निबन्ध की समीक्षा