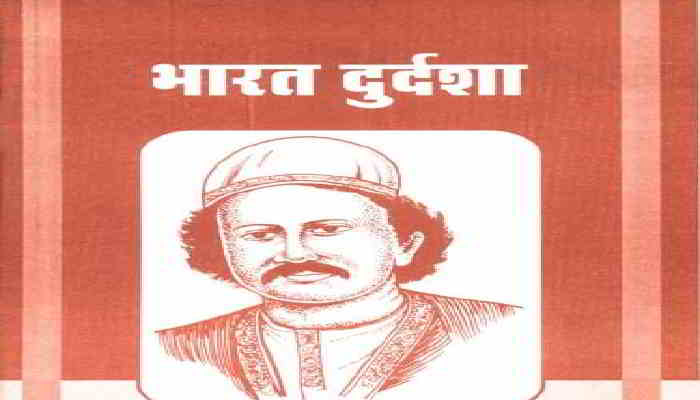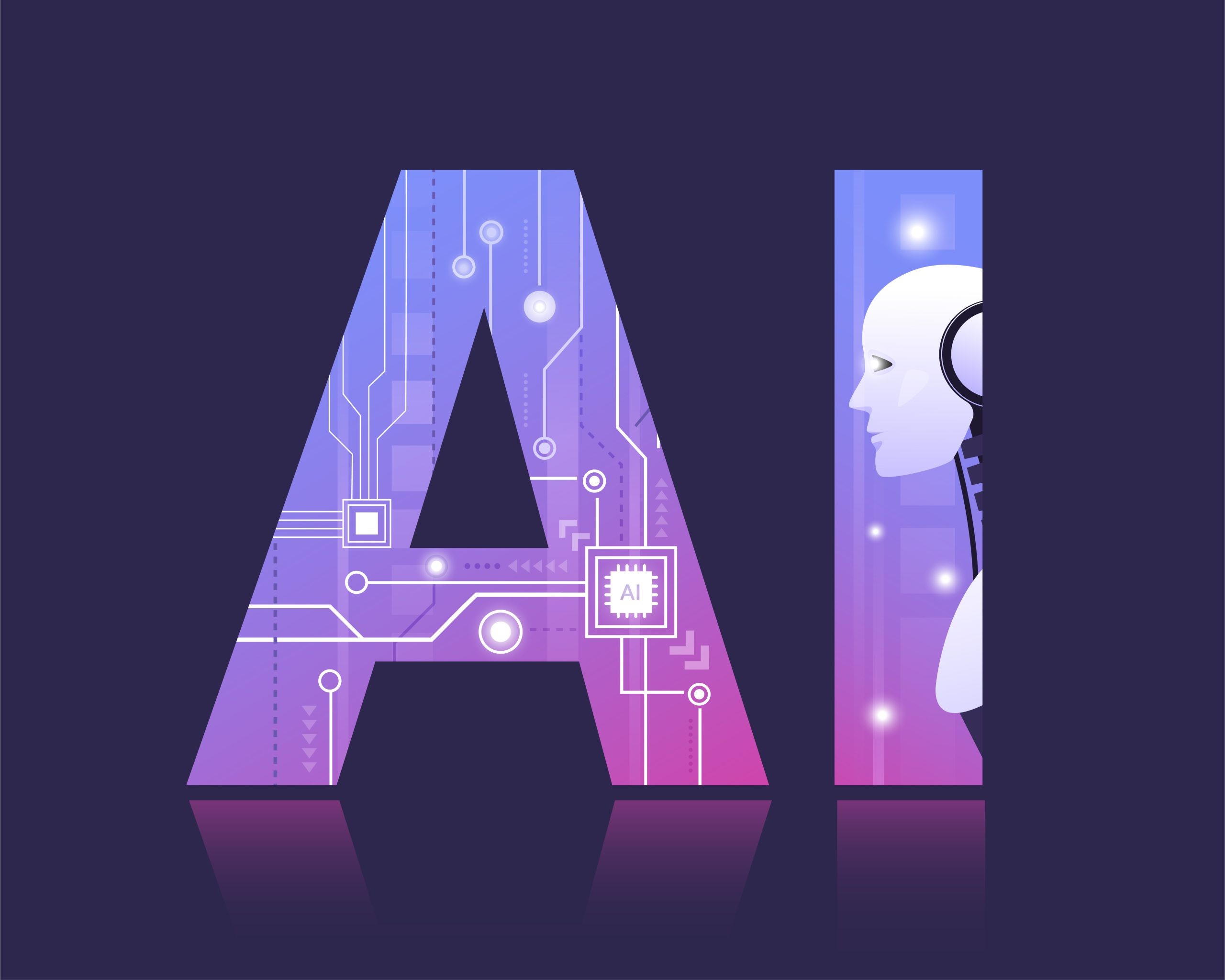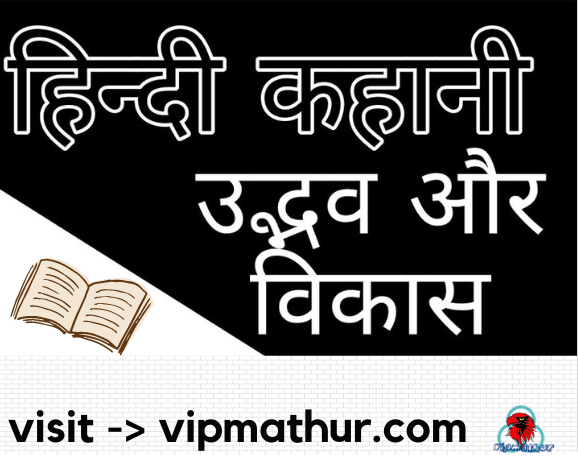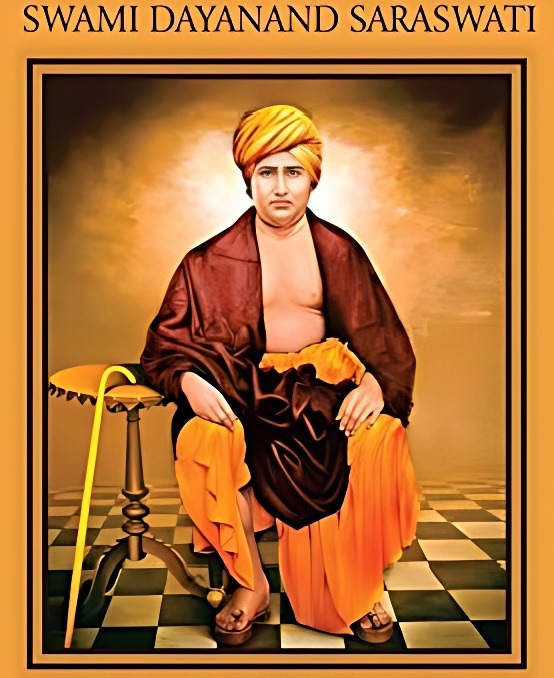भारत-दुर्दशा
भारत-दुर्दशा की मूल संवेदना -> भारत-दुर्दशा में भारतेंदु ने युग की राजनैतिक गतिविधियों सामाजिक परिस्थितियों और भारतीयों द्वारा अंग्रेजी सभ्यता. के गुणों को छोड़कार दुष्प्रवृत्तियों को अपनाया है। सामाजिक अंधविश्वासों और अज्ञान तथा असंगठित प्रवृत्तियों में फंसे रहने की उन समस्त समस्याओं का सजीव चित्रण किया है, जिने भारत उस समय ग्रसित था और इसके लिए उन्होंने अपने नाटक का नायक भारत को बनाया है। उन्होंने भारत के माध्यम से उन सभी समस्याओं को प्रतीक पात्रों के रूप में चित्रित किया है, जिनके कारण भारत-दुर्दुशा के कगार पर पहुँचा। इस प्रकार ‘भारत-दुर्दशा’ में नाटककार ने अपने युग का प्रत्यक्ष, यथार्थ एवं जीवंत प्रतिबिंब प्रस्तुत किया है।
भारतेन्दु युग के सच्चे एवं राष्ट्रवादी साहित्यकार थे। इसमें भी दो राय नहीं हक कि उनका पूरा झुकाव हिन्दू राष्ट्रवादिता की ओर था। पर वे राजभक्त तथा देशभक्त दोनों ही थे। राजभक्त से बड़े देशभक्त क्योंकि राजभक्त होते हुए ब्रिटिश साम्रज्य में जो उन्हें बुरा लगा उसका जबदस्त विरोध भी किया। डॉ. कृष्णदेव शर्मा कहते है… उनकी राजभक्ति और देशभक्ति की सीमाएँ हैं। कर्त्तव्य और संस्कारवश वह राजभक्ति प्रकट करते है । परिस्थिति के अनुसार अर्थात 1857 की क्रांति और 1858 के घोषणा-पत्र आदि के प्रकाशन में वैध रूप से अपने आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए राजकीय सहयोग माँगते हैं, अंग्रेजों के ज्ञान-विज्ञान की सराहना करते हैं पर साथ ही उनके आर्थिक-शोषण के विविध साधनों पर खुलकर व्यंग्य भी करते हैं।
भारत-दुर्दशा की मूल संवेदना
प्रेस एक्ट और गुण हाकिमेच्दा नामक दफा पर आक्षेप भी करते है, निरंकुशता के विरुद्ध खड़े होकर सवाल-जवाब करने साहस भी दिखते हैं, इसी प्रकार उनकी देशभक्ति की भी सीमाएँ हैं। समस्त विचार श्रेष्ठ हैं, यह देश केवल भारतियों का है, विदेशी लोगों का सहयोग हमें अपनी भलाई के लिए भी नहीं लेना है। विरोध ओर क्रांति ही हमारा मार्ग होना चाहिए, इस प्रकार की देशभक्ति उन्हें मान्य नहीं हैं। धर्म वह है, जो समय के अनुसार नवीनता ग्रहण करता हुआ समाज की रक्षा करें, विदेश शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में उर्वरक एवं रम्य बना सकते हैं-ऐसी देशभक्ति उन्हें मान्य थी।
‘भारत दुर्दशा’ में व्यक्त उनकी राष्ट्रीय भावना इसी श्रेणी की है।” डॉ जयनाथ नलिन लिखते हैं-“भारत दुर्दशा अतीत गौरव की चमकदार स्मृति है, आँसू-भरा वर्तमान है और भविष्य-निर्माण की भव्य प्रेरणा है। इसमें भारतेंदु का भारत प्रेम करुणा की सरिता के रूप में उमड़ चला आया है। आशा की किरण के रूप में झिलमिला उठा है।” युग चेतना एवं राष्ट्रवादी नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद जानते थे कि जब तक भारतीय जनता इस जड़ता और बुराइयों से छुटकारा लेकर राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना में प्रतिष्ठित नहीं होती, तब तक देश का उद्धार संभव नहीं। और “भारत-दुर्दशा में यही दृष्टिकोण काम कर रहा है। अतः भारतेन्दु युग-प्रवर्तक तथा राष्ट्रवादी थे, भलें ही उनकी राष्ट्रवादिता हिन्दू राष्ट्रवादिता ही हो।”
भारत-दुर्दशा की मूल संवेदना
भारत दुर्दशा’ में उनका यह प्रयास प्रमुखता से मिलता है। इस ग्रंथ में उन्होंने प्रतीकात्मक पात्रों द्वारा देश की दुरावस्था और दुर्भाग्य का मार्मिक चित्रण किया है। इस नाटक रचनाकाल 1880 है। यह वह समय था, जब महारानी विक्टोरिया ने ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ से भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया था। महारानी के आश्वासनों के बावजूद देश का हर तरह से शोषण हो रहा था। भारतीयों के हृदय में भी अंग्रेजों के शासन के प्रति कुछ विश्वास जमने लगा था।
कुछ उदार प्रकृति के अंग्रेज़ भारतीयों को स्नेह भी दे रहे थे। पर इसमें कुछ निश्चितता या स्थितरता का भाव नहीं था, भारतीयों में संगठन की कमी थी। अशिक्षा एवं अज्ञान के कारण के कुंठित हो रहे थे। सच्चा राष्ट्रवादी साहित्यकार इस स्थिति को अनदेखा नहीं कर सकता था, भारतेन्दु भी नहीं। अतः ‘भारत दुर्दशा’ में भारतेंदु ने अपनी इस सभी भावनाओं को स्पष्ट और निश्छल-भाव से अभिव्यक्त किया है।
एक राष्ट्रीय साहित्यकार देश में व्याप्त स्वास्थ नीति का समर्थन करता ही है। अतः भारतेंदु ने भी अंग्रेजी-शासन के साथ आई नई सभ्यता, वैज्ञानिक दृष्टि तथा उनकी उपलब्धियों का समर्थन किया। और भारतीय से उन नीतियों को अपनाने का आग्रह किया है । पर दूसरी और अंग्रेज-सत्ताधारियों की निरंकुशता का विरोध किया। वै इस नाटक के माध्यम से अंग्रेजों का आलोचना करते हैं, जिसके तहत भारतीयों पर बिना किसी ठोस नीति के अत्याचार किया जाता है।
भारत-दुर्दशा की मूल संवेदना
वस्तुतः भारतेंदु के मन में भारत की तत्कालीन दशा का गहरा क्षोभ था। हिंदू धीरे-धीरे पतन के गर्त के गिरते जा रहे थे। इसलिए वे पतन के गर्त से निकलने के लिए उन्हें उद्बोधित करने में रत थे। इसलिए वे कहते हैं-हिन्दुओ। तुम कहाँ थे और कहाँ आ पड़े हो। इसी तरह भरतवाक्य कहता है-” हा दैवा! तेरे विचित्र चरित्र हैं, जो कल राज करता था वह आज जूते में टांका उधार लगवाता है…..पवित्र चरित्र के लोग हो गए हैं उसकी यह दशा। योगी को माध्यम नाटककार भारत के स्वर्णिम अतीत को यों स्मरण करता है”
भारत-दुर्दशा” में राष्ट्रीय-भावना की सशक्त अभिव्यक्ति को देखकर डॉ. रमेश गौतम कहते हैं-“भारतेन्दु हश्चिंद्र की राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति का सुदर रूप ‘भारत दुर्दशा’ में परिलक्षित होता है। तत्कालीन जीवन की सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन की यथार्थ प्रतिकृति उनके प्रस्तुत नाटक में मुखरित हुई है।” डॉ. लक्ष्मीनगर वाष्णेय “भारत दुर्दशा” में अभिव्यक्त भारतेन्दु की राष्ट्रीयता-भावना की प्रशंसा करते हुए कहते हैं-” भारत दुर्दशा की कथा देश-वात्सलता और देश-हितैषिता का आदर्श-उदाहरण है। नवोत्थान-काल में उत्पन्न हेने के कारण भारतेन्दु देश के अतीत गौरव की भावना से अनुप्रणित थे ही साथ ही अपने चारों और उसकी महान् देश की अधोगति देश रहे थे।”
डॉ. गोपीनाथ तिवारी ने भारतेन्दु की राष्ट्रीयता को हिन्दू राष्ट्रीयता कहा है। उसके शब्दों में भारतेन्दु जी की राष्ट्रीयता है।